भारतीय जेलों में उभरता मानसिक स्वास्थ्य संकट
भारतीय जेलों में आत्महत्याओं की दर, आम जनसंख्या की आत्महत्या दर की तुलना में बहुत अधिक है। फिर भी इन जेलों में अधिकांश मनोचिकित्सक के पद खाली हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा बी बहुत कम है।
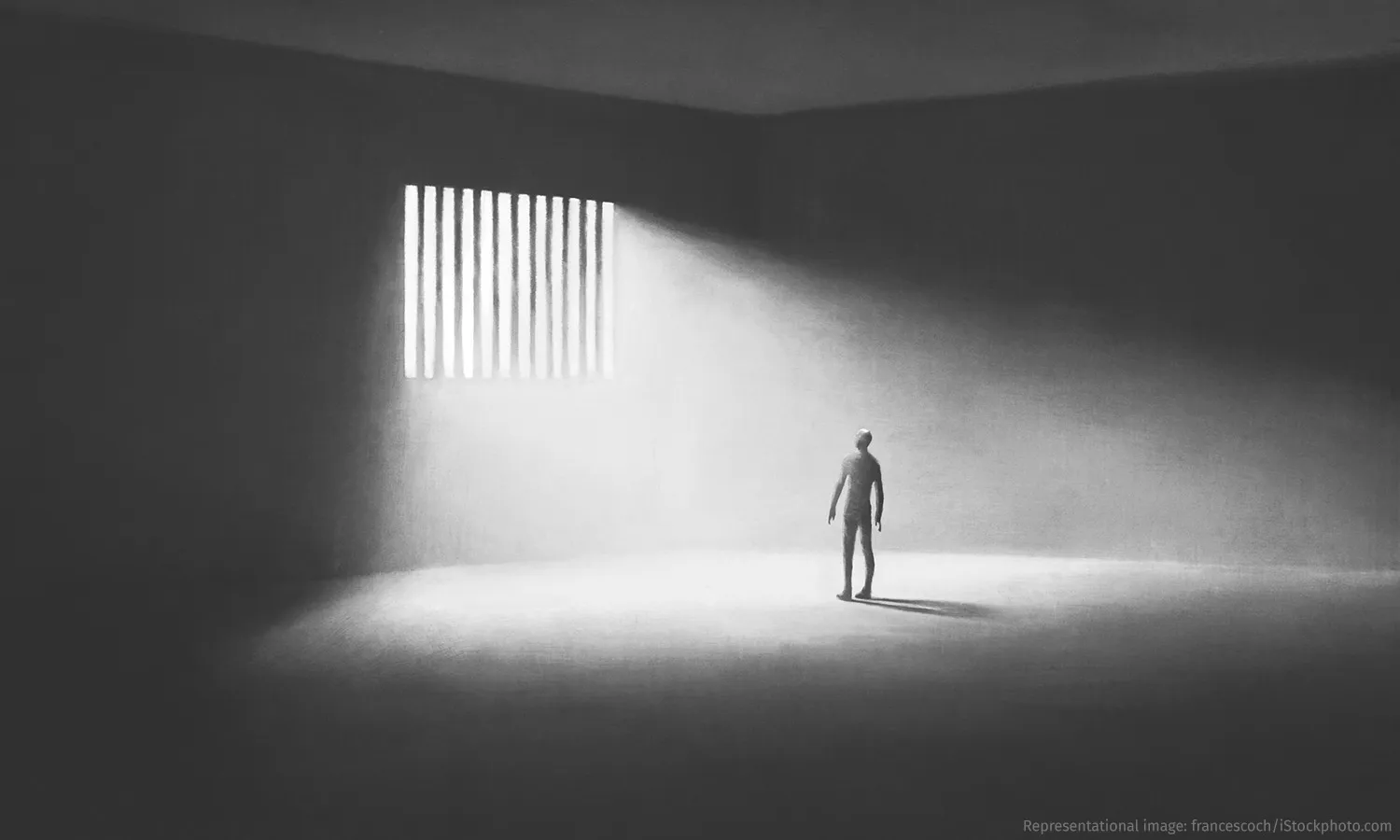
चेतावनी: इस स्टोरी में आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का उल्लेख है
बेंगलुरु: भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादियों में से एक है। इनमें ज्यादातर विचाराधीन कैदी हैं और वे हाशिये पर रहने वाले समुदायों से आते हैं। इसके बावजूद जेलों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो सीमित सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं, वे पहले से ही एक गंभीर संकट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों और कुछ स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार असल स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित आखिरी 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 119 कैदियों ने आत्महत्या की। यह हर एक लाख कैदियों पर 20.8 आत्महत्याओं की औसत है, जो सामान्य राष्ट्रीय औसत से 67 प्रतिशत ज्यादा है। 2014 से 2022 तक की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' रिपोर्ट्स के विश्लेषण से ये प्रमुख बातें सामने आई हैं:
• 2022 में 573,220 कैदियों में से कम से कम 9,084 यानी 1.6 प्रतिशत कैदियों ने मानसिक बीमारी की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के 'सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग' के अनुसार 2023 तक यह संख्या बढ़कर 16,503 हो गई।
• 2017 से 2022 के बीच जेलों में हुई अप्राकृतिक मौतों में से लगभग 80 प्रतिशत, यानी 980 में से 779 मौतें आत्महत्या के कारण हुईं।
• 2022 में जेलों में मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के लिए स्वीकृत पदों में से तीन में से दो पद खाली थे। यह 2016 के बाद से सबसे ज्यादा औसत है। सिर्फ 2018 एकमात्र साल था, जब 50 प्रतिशत से ज्यादा पद भरे गए थे।
• 2022 में जेलों में केवल नौ महिला मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक काम कर रही थीं, जिनमें से छह अकेले तमिलनाडु में थीं।
विशेषज्ञों ने इंडिया स्पेंड को बताया कि जेलों में मानसिक बीमारी उतनी सीमित नहीं है, जितना कि NCRB के आंकड़े दिखाते हैं। संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण के अभाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं और ज़रूरी देखभाल की प्रभावी निगरानी, ऑडिट और मूल्यांकन नहीं हो पाता है।
क़ानूनी शोध थिंक-टैंक पैक्टा की जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने भी बताया कि भारतीय जेल व्यवस्था में मानसिक बीमारियों व अन्य अक्षमताओं से जुड़ा अपडेटेड डेटा न होना, सुधारों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है।
सरकारी आंकड़े त्रुटिपूर्ण या कम क्यों हैं?
कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जेलों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। कोविड-19 के दौरान कैदियों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को संबोधित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) द्वारा 2021 में प्रकाशित एक अध्य्यन पुस्तिका में 2011 से 2014 के बीच किए गए कई अध्ययनों का हवाला दिया गया। इन अध्ययनों में पाया गया कि विभिन्न राज्यों के जेलों में मानसिक बीमार कैदियों की मौजूदगी 23.8% से 82% के बीच थी, जो कि 2022 के आधिकारिक जेल आंकड़ों से कम से कम 10 गुना ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश में मानसिक बीमारी से ग्रस्त कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जो कुल कैदियों का 23 प्रतिशत थी। इसके बाद केरल और ओडिशा का स्थान रहा, जहां मानसिक बीमारी से ग्रस्त कैदियों की संख्या क्रमशः 9 प्रतिशत थी।
मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस सेंटर में प्रोफेसर विजय राघवन बताते हैं कि मानसिक बीमारी का प्रसार NCRB के जेल आंकड़ों में जितना दिखाया गया है, उससे कहीं ज्यादा है।
बेंगलुरु स्थित NIMHANS के मनोरोग विभाग और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैबोरेटरी के प्रोफेसर संजीव जैन ने इंडिया स्पेंड को बताया, "जेलों में कम से कम दो-तिहाई लोग चिंता, निराशा और अवसाद से जूझ रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह जेल के माहौल की वजह से है या इसलिए कि सजा के समय कैदियों का मानसिक परीक्षण नहीं किया जाता। हमारे पास कोई शुरुआती डेटा नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "अक्सर युवा कैदी परेशान पारिवारिक जीवन से आते हैं और सामाजिक बहिष्करण का सामना करते हैं। जब कानून से पहली बार उनका सामना होता है, तब वे मानसिक बीमारी के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाते हैं।"
NIMHANS द्वारा 2011 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 5,000 से अधिक कैदियों के लिए सिर्फ एक मनोचिकित्सक था। अध्ययन में बताया गया कि MINI मापदंडों के अनुसार, 4,002 कैदियों यानी 79.6% लोगों को मानसिक बीमारी या नशे की आदत के साथ पहचाना गया।
नशे की लत को हटा भी दिया जाए तो हर चार में से कम से कम एक कैदी को मानसिक बीमारी थी। लगभग 12.7% कैदियों को जीवन में कभी न कभी गहरे अवसाद का सामना हुआ था और 9.1% उस समय सक्रिय अवसाद में थे, जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में दो गुना ज्यादा था।
अध्ययन में यह भी बताया गया कि हर 100 में से दो कैदियों ने आत्महत्या की कोशिश की थी और 100 में से सात से ज्यादा ने जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाया था। इसमें कहा गया, "केवल 2% कैदियों ने ही मानसिक बीमारी की खुद से रिपोर्ट दी थी। इससे यह समझा जा सकता है कि एक व्यवस्थित मूल्यांकन से मानसिक बीमारी की पहचान 14 गुना बेहतर हो सकती है।"
तेलंगाना के एक जेल अधिकारी ने राज्य के उन आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती दी, जिनमें कहा गया है कि राज्य के सिर्फ 2% कैदियों को ही मानसिक बीमारी है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने इंडिया स्पेंड को बताया कि असल में संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई कैदी दवाइयों पर हैं और गंभीर मामलों को राज्य के मानसिक अस्पतालों में भेजा जाता है।
अधिकारी ने बताया कि राज्य की जेल व्यवस्थाएं, नागरिक संगठनों से आए स्वयंसेवक परामर्शदाताओं पर निर्भर करती हैं। नए आने वाले कैदी अविश्वास के कारण मानसिक समस्याएं साझा नहीं करते, जबकि केवल गंभीर मामलों की पहचान कर इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा, "अगर जेल का चिकित्सा स्टाफ ये सेवाएं दे, तो इससे निरंतरता बनी रहेगी और कैदियों के साथ भरोसा भी बनेगा।"
संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक नियम, जिन्हें नेल्सन मंडेला नियम (नियम 30) भी कहा जाता है, सिफारिश करते हैं कि जेल में दाखिले के समय कैदियों की स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं की जांच की जानी चाहिए।
हर 23,000 कैदियों पर सिर्फ 1 मानसिक स्वास्थ्य कर्मी
देशभर की 1,330 जेलों में 5,70,000 से अधिक कैदियों के लिए 2022 में सिर्फ 25 मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक काम कर रहे थे—यानी हर 23,000 कैदियों पर सिर्फ एक विशेषज्ञ।
उसी साल भारत के 36 में से 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मनोवैज्ञानिकों या मनोचिकित्सकों के लिए एक भी पद स्वीकृत नहीं किया था। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल थे—जहां देश की 40% से ज्यादा जेल आबादी रहती है और जहां जेलों की भीड़ राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।
यूरोपियन यूनियन के 30 सदस्य देशों के हेल्थ इन प्रिज़न्स यूरोपियन डेटाबेस के अनुसार वहां पर हर 1,000 कैदियों पर 1.4 मनोचिकित्सक थे। इसके विपरीत 2022 की जेल संबंधी भारतीय आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 1,000 कैदियों पर सिर्फ 0.05 मनोचिकित्सक थे।
यह 2016 के मॉडल प्रिजन मैन्युअल से भी पीछे है, जिसे गृह मंत्रालय ने जारी किया था। इसमें कम से कम हर 500 कैदियों पर एक मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता रखने की सिफारिश की गई है। लेकिन यह मैन्युअल केवल एक दिशा-निर्देश है और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है और जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों के अधीन होता है।
हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 यह अनिवार्य करता है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और जेलों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को "बुनियादी और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल" प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करें। इसमें यह भी कहा गया है कि हर राज्य की कम से कम एक जेल के चिकित्सा विभाग में एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जून 2023 में एक सलाह जारी कर राज्य सरकारों से मौजूदा खाली पद भरने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, जेल कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित करने, हर तीन साल में रिफ्रेशर कोर्स शामिल करने, जोखिम में रहने वाले कैदियों की जांच व निगरानी करने और गेटकीपर मॉडल को लागू करने की सिफारिश की। इस मॉडल के अनुसार जेल के ही कुछ कैदियों को जोखिम में पड़े लोगों की पहचान करने और उन्हें रेफर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
NIMHANS के जैन ने कहा कि हर जेल में एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक होना चाहिए, लेकिन ये पद कभी नहीं भरे जाते हैं। TISS के राघवन ने कहा कि अगर मनोचिकित्सक के पद खाली हैं, तो राज्य सरकारों को कम से कम अनुबंध पर सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता नियुक्त करने चाहिए ताकि वे रोकथाम पर केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल दे सकें।
हैदराबाद स्थित NALSAR विश्वविद्यालय के स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय की निदेशक मैत्रेयी मिश्रा ने कहा कि अधिकतर राज्यों के जेलों में कोई प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य जांच या समय-समय पर मूल्यांकन नहीं होता। उन्होंने बताया, “एक हेल्थ प्रोफॉर्मा होता है जो कैदियों के जेल में प्रवेश के समय भरा जाता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित केवल एक सामान्य सवाल होता है।”
मिश्रा ने बताया कि जिन जेलों में वह गई हैं या जिनकी जानकारी उनके पास है, उनमें NHRC की गाइडलाइंस लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “गाइडलाइंस खुद ही काफी नहीं हैं क्योंकि वे बहुत अस्पष्ट हैं और पता नहीं इसका कितना हिस्सा प्रमाण आधारित है। जहां ये गाइडलाइंस लागू भी हो रही हैं, वहां भी नहीं पता कि उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा हो रही है या नहीं। हमारे पास आत्महत्या की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी नीति नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च एंड प्लानिंग सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जेल विभागों ने सकारात्मक रूप से उत्तर दिया कि नवप्रवेशी कैदियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में मानसिक स्वास्थ्य जांच भी शामिल होती है। लेकिन अलग-अलग राज्यों में जांच का तरीका अलग-अलग था। ओडिशा की अधिकतर जेलों में नए कैदियों की जांच एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सायकेट्रिक सोशल वर्कर द्वारा की जाती है, जबकि गुजरात, पुडुचेरी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए कैदियों की व्यवहारिक जांच, जेल मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाती है।
केरल, जम्मू कश्मीर और मणिपुर ने बताया कि नए कैदियों के स्वास्थ्य की जांच तो होती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं है।
रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि ज्यादातर राज्यों में स्वास्थ्य जांच मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाती है। ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड की कुछ जेलों को छोड़कर अधिकतर जेलों के मेडिकल ऑफिसर्स को बुनियादी और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 31(2) का उल्लंघन है।
जेलों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और पीयर नेटवर्क
मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 को मई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझा किया गया था। इस एक्ट को जेलों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इसमें प्रावधान है कि मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बताया गया कि केवल छह राज्यों (असम, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा) और एक केंद्र शासित प्रदेश (लद्दाख) के जेलों में ही मानसिक रूप से बीमार कैदियों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
राज्य के मानसिक स्वास्थ्य तंत्र में मौजूद खामियों के चलते कुछ जेलों ने पीयर नेटवर्क का सहारा लिया है। तेलंगाना की “उन्नति” और गुजरात की “समर्थ” जैसी पहलों में कैदियों के व्यवहारिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहां पीयर काउंसलिंग के जरिए मदद की जाती है।
तेलंगाना के एक जेल अधिकारी ने इंडिया स्पेंड को बताया कि राज्य के जेलों में मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की कोई उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है। जिला अस्पतालों के मनोचिकित्सक साप्ताहिक रूप से कैदियों की जांच के लिए आते हैं और नागरिक समाज संगठन कैदियों व कर्मचारियों को जोखिम में पड़े लोगों की पहचान करना सिखाते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हो सकते हैं, जो आम लोगों की नजर में नहीं आते।
इंडिया स्पेंड ने गृह मंत्रालय से यह पूछने के लिए संपर्क किया है कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों में मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए कोई पहल की है, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, निगरानी, आत्महत्या की रोकथाम और कैदियों की स्क्रीनिंग शामिल है। जब उनका जवाब मिलेगा, तो इस स्टोरी को अपडेट किया जाएगा।
प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार, मानसिक बीमारी वाले 9,084 कैदियों में से लगभग 63% विचाराधीन कैदी थे। हालांकि सजायाफ्ता कैदियों में मानसिक बीमारी का प्रसार अधिक होता है, लेकिन विचाराधीन कैदियों पर अनिश्चितता व तत्कालिक मानसिक दबाव उन्हें विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट “प्रिजन्स एंड हेल्थ” बताती है कि रिमांड पर रखे गए बंदी, विशेष रूप से जिन्हें एकांत में रखा गया हो, अधिक संवेदनशील होते हैं।
द स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की मिश्रा ने कहा, “भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है। शोध से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन कैदी, विशेष रूप से नए कैदी, सजायाफ्ता कैदियों की तुलना में आत्महत्या का प्रयास करने की अधिक संभावना रखते हैं। हालांकि फिर भी इनके लिए कोई विशेष नीति नहीं है, जो उनकी विशेष समस्याओं को संबोधित करे।”
महिला कैदियों के पास नहीं के बराबर आधारभूत सुविधाएं
जेलों में एक और संवेदनशील समूह महिलाओं की है। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन जेल की स्थितियां, खासकर छोटे बच्चों के साथ वाली महिला कैदियों की परिस्थितियां उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं, जैसा कि इंडिया स्पेंड ने पहले रिपोर्ट भी किया है।
TISS के विजय राघवन ने इंडिया स्पेंड को बताया कि निम्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति, अकेलापन, बच्चों तक पहुंच का खो जाना और पारंपरिक समाजों में सामाजिक भूमिका का खत्म हो जाना, जेल में बंद महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।
2016 की मॉडल प्रिजन मैनुअल में सिफारिश की गई है कि हर जेल में कम से कम एक महिला मनोचिकित्सक नियुक्त की जाए। इसका मतलब है कि 16 राज्यों में मौजूद 34 महिला जेलों के लिए कम से कम 34 महिला मनोचिकित्सक हों। लेकिन 2022 में पूरे देश में केवल नौ महिला मनोचिकित्सक नियुक्त थी, जिनमें से छह तमिलनाडु में थीं।
महिला कैदियों और गैर-हिरासत में रहने वाली महिला अपराधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम (बैंकॉक नियम) कहते हैं कि महिलाओं को लिंग आधारित स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए, जो कम से कम समुदाय में उपलब्ध सेवाओं के बराबर हों।
मानसिक स्वास्थ्य संकट पूरी दुनिया की जेलों को प्रभावित कर रहा है
2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 50 से अधिक उच्च, मध्यम और निम्न आय वाले देशों के आंकड़ों और प्रमुख अध्ययनों को एकत्र कर समीक्षा और विश्लेषण किया। इस अध्ययन में पाया गया कि जेलों में डिप्रेशन और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD की दर बहुत अधिक है। इसके साथ ही नशे और शराब की लत से जुड़ी बीमारियों की दर भी बहुत अधिक है।
अध्ययन में बताया गया कि 11.4 प्रतिशत कैदियों को डिप्रेशन था, जबकि आम आबादी में यह दर 6 से 8 प्रतिशत के बीच है। इसके अलावा 9.8 प्रतिशत को PTSD और 3.7 प्रतिशत को मानसिक भ्रम या साइकोटिक डिसऑर्डर था। यह दर भी आम आबादी की तुलना में कम से कम दो गुनी अधिक थी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के 2021 के ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार, 2000 से 2019 के बीच 6,200 से अधिक स्थानीय जेल कैदियों ने आत्महत्या की। इस बीस साल की अवधि में जेलों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आत्महत्या करने वालों में से तीन चौथाई से अधिक लोग मुकदमे का फैसला होने का इंतजार कर रहे थे और दोषी सिद्ध नहीं हुए थे।
यह संकट जारी क्यों है?
NIMHANS के जैन बताते हैं, “पहले चिकित्सा प्रणाली नागरिक व्यवस्था से जुड़ी होती थी और न्यायिक व कानूनी तंत्र के साथ समन्वय से काम करती थी, लेकिन अब ये सेवाएं अलग हो चुकी हैं। अब जो डॉक्टर जेल सेवा में शामिल होता है, उसे बाहर के किसी तंत्र से संपर्क नहीं रखना होता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी सब अलग-अलग हो गए हैं, जिससे जेल के चिकित्सा पेशेवरों के लिए विकास के रास्ते कम हो गए हैं और उनके लिए प्रोत्साहन की भी कमी है।”
अपराध न्याय पर केंद्रित TISS की पहल ‘प्रयास’ के प्रमुख राघवन ने ऐसे कई तनाव के कारणों की ओर इशारा किया, जिससे कैदी अवसाद ग्रसित होते हैं। इसमें परिवार का सहयोग न मिलना, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जेल की रोजमर्रा की प्रक्रियाएं- जैसे रोज का निरीक्षण या आपात स्थिति में अलार्म बजना शामिल है। ये स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो सकती हैं।
पुणे स्थित इंडियन लॉ सोसाइटी के सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के सह-निदेशक और वरिष्ठ शोधकर्ता कौस्तुभ जोग ने कहा कि विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समूहों से आने वाले लोगों के लिए अनिश्चितता और सीमित कानूनी संसाधन, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
मृत्यु दंड पाने वाले कैदियों की मानसिक स्थिति पर अध्य्यन कर चुके जोग ने कहा कि जेलों में अक्सर ऐसे पदानुक्रम होते हैं, जो भेदभाव और उत्पीड़न को जन्म देते हैं। इससे मानसिक पीड़ा और बढ़ जाती है व आत्महत्या का विचार अवसाद के बिना भी आ सकता है। यह अचानक आने वाले भावनात्मक झटके से शुरू हो सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता के अलावा जोग ने जैव-चिकित्सकीय पद्धति से आगे बढ़कर देखभाल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है, जिसमें स्वच्छता, भोजन, मनोरंजन की सुविधाएं और व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं।
2011 की NIMHANS की रिपोर्ट के अनुसार, “जेल स्वास्थ्य की अक्सर उपेक्षा की जाती है और यह अनदेखी आज बी जारी है। जबकि इस क्षेत्र में उपलब्ध ठोस आंकड़े और प्रमाण यह दिखाते हैं कि जेलों में ठोस स्वास्थ्य नीतियों की ज़रूरत है। राजनेता, नीति निर्माता, नौकरशाह और सामुदायिक नेता इस क्षेत्र को नज़रअंदाज़ करते आए हैं। इसके लिए वे तरह-तरह के कारण बताते हैं, जैसे- ‘कैदियों को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है’, ‘उन्हें कष्ट सहने दो’, ‘पर्याप्त फंड नहीं हैं’ या ‘प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं’ इत्यादि।
अगर आप मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं या आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो मदद उपलब्ध है। कृपया किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या अपने नजदीकी हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
इंडियास्पेंड में इंटर्न अश्विन श्रीकुमार ने इस स्टोरी के आंकड़ों को जुटाने में मदद की है।
इस स्टोरी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। कृपया हमें respond@indiaspend.org पर लिखें। हम भाषा और व्याकरण की शुद्धता के लिए आपके प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार रखते हैं।

